जनवादी नाटककार राजेश कुमार का जन्म 11 जनवरी 1958 पटना, बिहार में हुआ। राजेश कुमार नुक्कड़ नाटक आंदोलन के शुरुआती दौर 1986 से सक्रिय है। अब तक दर्जनों नाटक एवं नुक्कड़ नाट्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आरा की नाट्य संस्था युवानीति, भागलपुर की दिशा और शाहजहाँपुर की नाट्य संस्था अभिव्यक्ति के संस्थापक सदस्य। पेशे से इंजीनियर रहे, सन् 2018 में UPPCL के लखनऊ कार्यालय से मुख्य अभियंता के पद से सेवा निवृत हुए। इन दिनो इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में निवास है। पेश हैं उनसे बातचीत के प्रमुख अंश :

आप उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन से मुख्य अभियंता के पद से सेवानिवृत हुए। एक तरफ इंजीनियरिंग का पेशा और दूसरी ओर नाटकों का लेखन। आप का साहित्य की ओर झुकाव कब और कैसे हुआ ?
मेरी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत कहानी लेखन से हुई थी। पहली कहानी ‘चुप रहने के लिए’ सन 1978 में उस वक्त की चर्चित हिंदी कहानी पत्रिका ‘सारिका’ में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद दूसरी कहानी ‘एक तबादला और’ सबसे बड़ी साहित्यिक पत्रिका ‘धर्मयुग’ में दो किस्तों में छपी थी। उसके बाद लगभग एक दर्जन कहानियां ‘कथन’, ‘ पुरुष’, ‘लहर’, ‘सक्रिय कहानी’ , ‘रूप कंचन’ जैसी बड़ी–लघु पत्र–पत्रिकाओं में निरन्तर छपी और साहित्यिक हलकों में अपने रूप और विषय को लेकर किसी न किसी रूप में चर्चा का विषय बनी रही। उन दिनों आरा शहर जहां मैं रहता था, साहित्यिक और राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय था। कथा साहित्य के क्षेत्र में युवा कथाकारों की एक बड़ी संख्या थी। भोजपुर के लहलहाते खेत–खलिहानों में उन दिनों किसानों के जागरण से भूमि आंदोलन में नए तरह का बदलाव देखने को मिल रहा था। उसकी उपस्थिति कथा में दीख रही थी, पर सांस्कृतिक पटल पर नदारद थी। वहां सामन्तों का आधिपत्य था। वही मूल्य नाच–गान व नौटंकी में सर्वोपरि पर था। ऐसे में मुझे बार-बार लगता था कि संस्कृति का यह कोना जो अभी भी उपेक्षित है, बदलने की जरूरत है।
एक तरफ यथार्थवाद के नाम पर रंगमंच पर पलायनवाद को सच बताने का अभिजात्य प्रयास चल रहा था तो दूसरी तरफ जड़वादी परंपरा के नाम पर पुरानी सड़ी–गली परम्पराओं को संस्कृति के नाम पर परोसने का कार्य कर रहा था। इस जड़ता को तोड़ने और बदलाव की जमीन से लोगों को रूबरू करने की जद्दोजहद कहीं न कहीं मन के अंदर व्याप्त थी, जिसका परिणाम ये निकल कर आया कि मैं कहानी लेखन से कब नाट्य लेखन और थिएटर एक्टिविस्ट के रूप में तब्दील हो गया, मुझे भी पता नहीं चला।
शायद सांस्कृतिक आंदोलन की जरूरत ने मुझे इस दिशा की तरफ मोड़ दिया, ये कहना ज्यादा सार्थक होगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने के पहले से मैं थिएटर से जुड़ा रहा था। बल्कि इसकी शुरुआत स्कूल के दिनों से ही हो गयी थी। इंटर पास करने के बाद तो मैं प्रतिबद्ध रूप से जुड़ गया था। उस वक्त का लगा रोग अभी तक है। नौकरी से रिटायर होने के बाद भी यह रोग नहीं गया है। और आगे शायद जाए भी नहीं। जब तक जिंदा हूँ, लगा ही रहेगा। कुछ रोग जानलेवा नहीं होते हैं , जीवन को बढ़ाने का काम करते हैं। थिएटर ऐसा ही एक प्राणदायक रोग है।

आपने नाट्य लेखन किया, अभिनय किया और नाट्य निर्देशन भी किया। लेखन से निर्देशन तक के इस सफ़र के बारे में बताइये।
रंगमंच में मेरी एंट्री बतौर एक्टर के रूप में ही हुई थी। पहले कॉलोनी के नाटकों में भाग लिया, फिर कॉलेज के। कुछ दिनों तक स्थानीय संस्थओं के साथ शौकिया रूप से थिएटर किया। करने के दौरान महसूस हुआ कि नाटक करना कोई शौकिया काम नहीं है। राजनीति करने व कोई सामाजिक कार्य करने जैसा ही थिएटर करना भी कोई कार्य है। थिएटर करना कोई टाइम पास करने जैसा काम नहीं है। यह एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां से कोई व्यक्ति अपनी कोई विचारधारा को कला के रूप में अभिव्यक्त कर सकता है। इसी जरूरत के तहत कुछ हमख्याल रंगकर्मियों ने आरा शहर में ‘युवा नीति’ के नाम से एक संस्था बनायीं।
उनदिनों शहर में जो भी नाटक होते थे, प्रशासकीय प्रेक्षागृहों में, किसी स्कूल–कॉलेज के ऑडिटोरियम में होते थे। वहां जो भी नाटक करते थे ... जिस प्रकार के भी नाटक करते थे, वो मध्यवर्गीय जन जीवन के इर्द–गिर्द का ही होता था। उस मंच पर शोषित–उत्पीड़ित समाज का जीवन उतारने का कोई ज्यादा स्पेस नहीं होता था। ऐसे लोगों पर नाटक देखने की इच्छा भी नहीं होती थी। ऐसे में हम लोगों ने नाटक को प्रेक्षागृहों से बाहर निकालने का निर्णय लिया। यह निर्णय केवल कोई प्रयोग के तहत नहीं था, चाहे तो इसे एक पोलिटिकल एफर्ट का नाम भी दे सकते हैं। और शायद वक्त का तकाज़ा भी था। यह वही दौर था जब देश में थोपे गए आपातकाल के विरोध में देश भर में कवि, कथाकार, गायक प्रतिरोध में अपनी–अपनी कलाओं के साथ नुक्कड़ों–चौराहों पर उतर रहे थे। कवि कविता पढ़ रहा था, पेंटर दीवारों पर चित्र बना रहा था, गायक डपली बजा कर गीत गा रहा था। सत्ता की निरंकुशता के विरोध में जनता के बीच बदलाव की एक नई जमीन तैयार कर रहा था। ऐसे में रंगमंच को तटस्थ रहना सम्भव नहीं था।
रंगमंच को जनता से जोड़ने और सीधा संवाद करने के उद्देश्य से हम प्रेक्षागृह से निकल कर सड़क पर आ गए। हमें कुछ पता नहीं था कि नुक्कड़ों पर नाटक कैसे किया जाता है। इसके व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं था। केवल यही जानते थे कि जनता के बीच जाना है। जनता के साथ जो शोषण - उत्पीड़न हो रहा है, उसे नाटक में लाकर लोगों को दिखाना है। उन्हें संगठित कर संघर्ष के लिए तैयार करना है। इस दशा में व्यक्तिगत रूप से मुझे कई भूमिकाओं को एक साथ निभाना पड़ता था। अगल–बगल घटनाएं घट रही थी, तात्कालिक मुद्दों पर नाटक तैयार करना पड़ता था। अभिजात्य रंगमंच से जुड़े एक्टर्स के नुक्कड़ों पर न उतरने से जो कलाकारों की कमी उत्पन्न होती थी, उसे दूर करने के लिए खुद आगे आना पड़ता था। निर्देशक के अभाव में यह जिम्मेदारी भी प्रायः खुद ही संभालनी पड़ती थी। अर्थात नुक्कड़ नाट्य आंदोलन में मैं लेखक, अभिनेता और निर्देशक के रूप में बराबर रूप से जुड़ा रहा।
यह सिलसिला इंजीनियरिंग की पढ़ाई तक तो चला ही, जब पावर कॉर्पोरेशन की नौकरी में आया, तो भी लंबे समय तक जारी रहा। झांसी, ओबरा, अनपरा और अलीगढ़ में नौकरी करने के उपरांत तबादले के बाद जब शाहजहांपुर आया तो रूप में बदलाव आ गया। यहां प्रोसेनियम थिएटर की एक मजबूत , लंबी परंपरा थी। अतः मंच पर काम करने लगा। और मेरी भूमिका बतौर लेखक और निर्देशक प्रमुख हो गयी। शाहजहांपुर में ग्यारह साल रहा। मेरे प्रमुख नाटक यहीं लिखे गए हैं। यहां का रंगमंच मेरे लिए प्रयोग की जमीन थी। जैसा मैं लिखना चाहता था, लिखा। जिस तरह उन नाटकों को निर्देशित करना चाहता था, स्वतंत्र होकर किया। यहीं मैंने क्रांतिकारियों की वैचारिकता को केंद्र में रख कर ‘आखिरी सलाम’ और ‘पगड़ी संभाल जट्टा’ जैसे नाटक लिखा। हाशिये के समाज पर रहने वालों पर ‘घर वापसी’, ‘हवनकुंड’, ‘सत भाषे रैदास’ जैसे नाटक लिखा। इन नाटकों में जिस तरह के सवाल उठाये गए थे, वंचित समाज को करीब से जोड़ा। मुख्य धारा के रंगमंच में एक बहस खड़ा किया। कलांतर में ‘दलित रंगमंच’ के लिए हिंदी क्षेत्र में इसने एक नई , पुख्ता जमीन तैयार की।
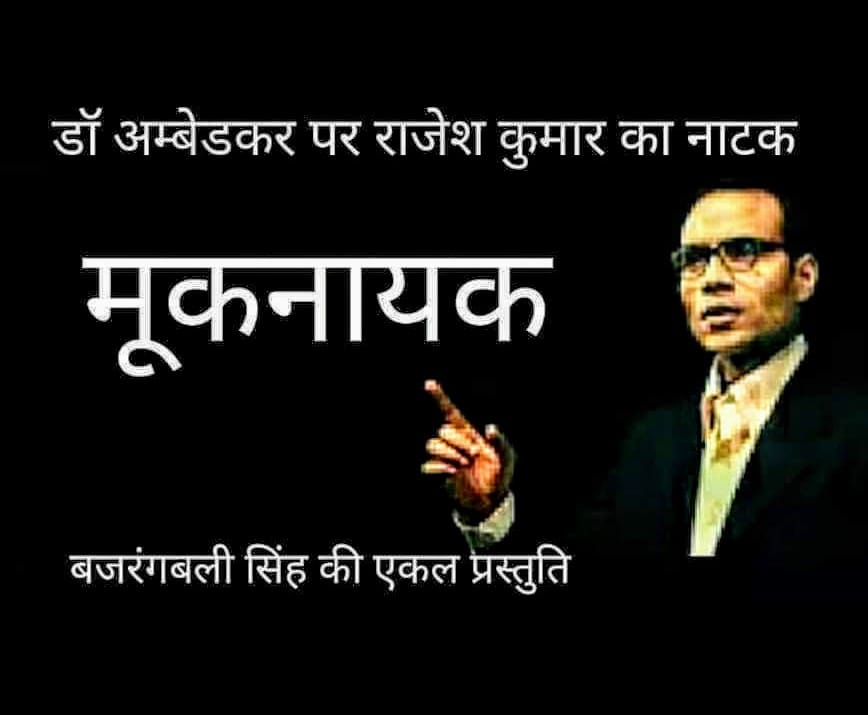
हाशिये पर रहने वाले वंचित समाज की बेचैनी, छटपटाहट को आपने नाटकों में प्रमुखता दी है। हाशिये के समाज को अपने लेखन में चुनने की क्या वजह रही ?
किसी एजेंडे या कोई राजनीतिक दल के दबाव के कारण अपने नाट्य लेखन में समाज के वंचित–उत्पीड़ित लोगों को नहीं लाया। सन 1990 के बाद हमारे देश में जो राजनीतिक बदलाव आया, दबे–कुचले लोगों में जो चेतना का भाव आया, सम्भवतः एक प्रमुख कारण था। दूसरी भाषाओं में इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गयी थी। उदाहरण के लिए अगर मराठी भाषा को ले तो वहां रंगकर्म में हाशिये का समाज आजादी के पहले से आ गया था। पिछली सदी के तीसरे दशक के आस–पास। अम्बेडकर उनदिनों समाज में व्याप्त अस्पृश्यता, जात–पात का भेद–भाव, धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास के खिलाफ जब सामाजिक आंदोलन चला रहे थे तो उसके असर से साहित्य–संस्कृति अलग नहीं रह सका। नाटक में भी वो सवाल मुखर होने लगे। वर्ण के आधार पर निम्न लोगों के साथ जो अमानुषिक अत्याचार होते थे, मंच पर चित्रित होने लगे।
अम्बेडकर सांस्कृतिक आंदोलन की ताकत अच्छी तरह से समझते थे। उन्हें भान हो गया था कि सांस्कृतिक आंदोलन की धार तेज किये बिना सामाजिक–राजनीतिक लड़ाई मजबूत, व्यापक नहीं की जा सकती है। इसलिए अम्बेडकर की भागीदारी उनदिनों ऐसे नाटकों में जरूर होती थी जिसमें हाशिये के समाज की उपस्थिति होती थी। सन 1936 में जब बॉम्बे थिएटर में ‘दक्खन का दीया’ नाटक मंचित हुआ था तो अम्बेडकर उसे देखने गए थे। उस नाटक में पेशवा राज में ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों से जो अमानवीय व्यवहार किया गया था, धर्म के बहाने जिस तरह जुल्म ढाया गया था, सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया गया था। नाटक को देखने इतने लोग आए थे कि हॉल में चींटी तक के लिए पैर रखने की जगह नहीं थी। तभी अम्बेडकर ने कहा था कि ‘मेरे दस भाषणों के बराबर एक नाटक है।‘

राजनीतिक–सामाजिक परिवर्तन के लिए सांस्कृतिक आंदोलन चलाना एक आवश्यक मुहिम है। अम्बेडकर के आंदोलन का प्रभाव केवल मराठी तक सीमित नहीं था। उस वक्त हिंदी साहित्य में भी उसका असर देख सकते हैं। अलबत्ता हिंदी रंगमंच असमंजस की स्थिति में जरूर था। गांधी और वामपंथ की तरह मुख्य धारा का रंगमंच भी वर्ण संघर्ष को वर्ग संघर्ष के सम्मुख अहमियत नहीं दे रहा था। उसने वर्ण–जाति की समस्या के सम्मुख साम्प्रदायिकता के सवाल पर ज्यादा जोर दिया। आपातकाल के दौर में भी सत्ता की निरंकुशता प्रमुख था। 90 के दशक में मंडल आयोग के आने पर जब दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों ने इसके विरोध में कमंडल को आगे लाया तो दबे–कुचले लोग जो अब तक हाशिये पर थे, राजनीति और संस्कृति में केंद्र में आने लगे। मेरे नाटकों में ऐसे विषयों के आने का यही कारण था।
एक बार आपने कहा था कि एक समय रंगमंच विपक्ष की भूमिका में था, लेकिन आज प्रतिरोध की ताकत कम हुई है। ऐसा आप क्यों मानते है ?
रंगमंच आज से ही नहीं, हमेशा से प्रतिपक्ष की भूमिका में रहा है। कोई भी राज हो, सत्ता के शीर्ष पर कोई भी राजनीतिक दल आसीन हो, रंगमंच जनता की तरफ होता है। उसका पक्ष लेता है। उसकी नब्ज होता है रंगमंच। समाज में जो भी घट रहा होता है, शोषण-अन्याय के विरुद्ध कोई भी बोल रहा होता है, रंगमंच सही मायने में उसका आईना होता है। अगर रंगमंच समाज से कट कर सत्ता या दरबार के हित में कला का सृजन करने लगे तो वो जनता का रंगमंच नहीं कहलायेगा। वो दरबारी संस्कृति का हिस्सा बन जायेगा। आजादी की लड़ाई में रंगमंच की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कि ऐसे नाटक खेले गए जो ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में था। यहां तक कि पारसी नाटक जो व्यावसायिक था, उसने भी अपने नाटकों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जगाने में एक सार्थक भूमिका अदा की थी। बंगाल के अकाल के दिनों में रंगमंच शोषित–पीड़ित लोगों की सबसे मजबूत आवाज के रूप में अखिल भारतीय स्तर पर उभर कर आई थी। नक्सलबाड़ी में किसानों की हथियारबंद लड़ाई और आपातकाल के विरोध में जो छात्र आंदोलन उभरा था, अभिजात्य रंगमंच से अलग नुक्कड़ नाटक ने जो स्टैंड लिया था, उसे समाज के हर लोगों ने सराहा था। जो बात विपक्ष उठा रहा था, नुक्कड़ नाटक आंदोलन उसे व्यापक रूप दे रहा था।
बाद में कहीं न कहीं सत्ता को यह नाट्यरूप नागवार लगा, जिसका यह परिणाम देखने को मिला कि नुक्कड़ नाटक या तो सत्ता की गोदी में जा बैठा या किसी एनजीओ का एजेंट बना दिया। आज तो और भी बुरा हाल है। विपक्ष की तरह रंगमंच भी कमजोर हो गया है। शहरी रंगमंच इतना महंगा हो गया है कि सरकारी ग्रांट या अनुदान लेना उसकी मजबूरी हो गयी है। जो प्रतिरोध की धारा से जुड़ कर नाटक कर रहे हैं, उन पर सत्ता का दमन इतना बढ़ गया है कि उनके लिए नाटक करना दूभर होता जा रहा है। सत्ता ने रंगमंच को इतना बांट दिया है कि उसी दायरे में अपने को सीमित कर समाज की समस्या को देखते और विश्लेषित करते हैं।
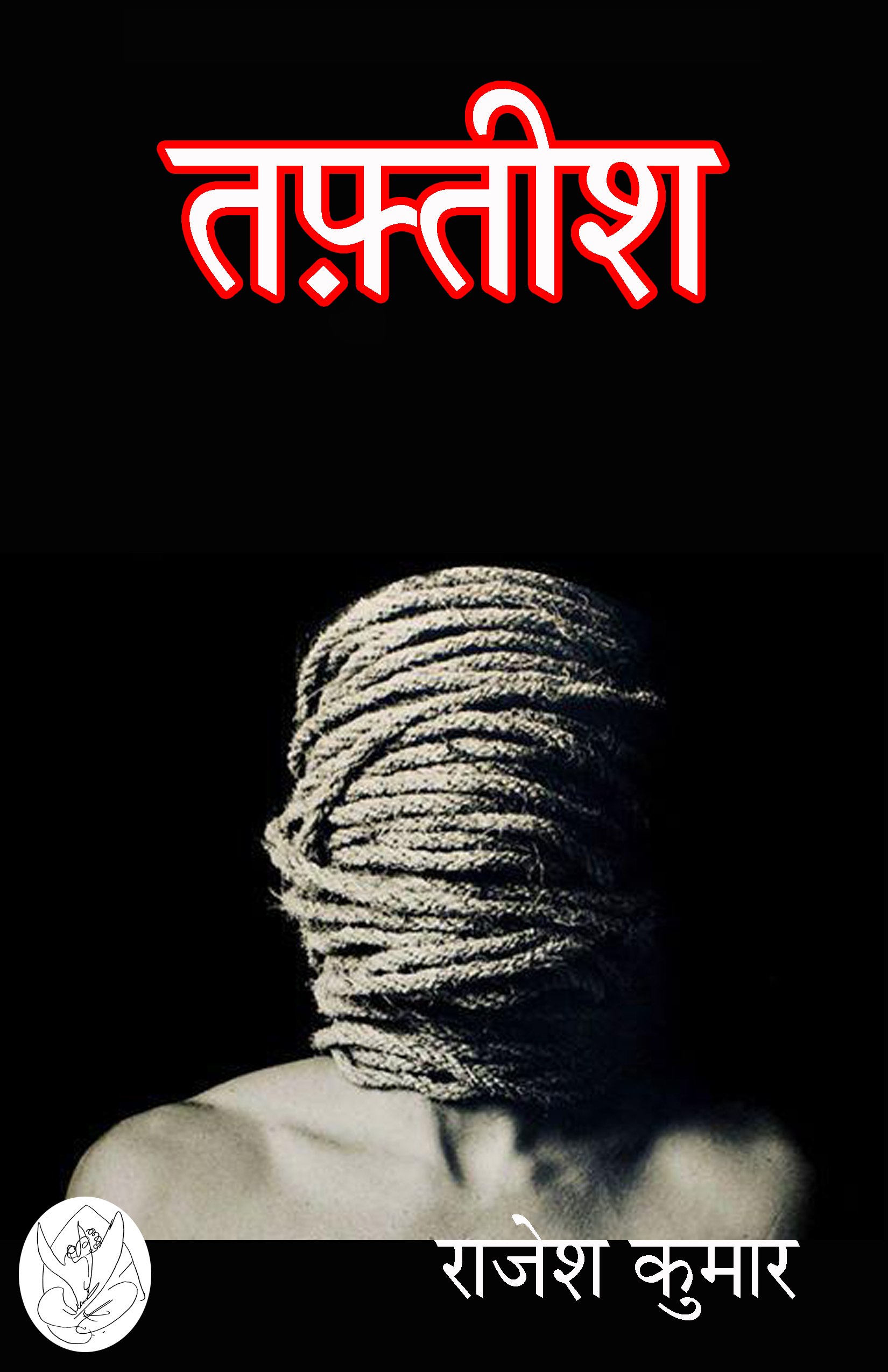
आपने अभी तक 24 नुक्कड़ नाटक और 22 पूर्णकालिक नाटक लिखे हैं। नुक्कड़ नाटक लिखने के पीछे क्या सोच रही है ?
प्रोसीनियम से नुक्कड़ की तरफ रुख मैंने किसी प्रयोग या रंगमंच में कुछ नया करने के लिए नहीं किया था। एक राजनीति के तहत आना हुआ था। सन 74 का जो दौर था, राजनीतिक रूप से काफी उथल–पुथल का दौर था। इसके कुछ वर्ष पूर्व नेहरू सरकार से मोहभंग होने पर नक्सलबाड़ी में जो किसान आंदोलन उठा था, उसने देश भर के साहित्यकारों–संस्कृतिकर्मी को वैचारिक रूप से प्रभावित किया था। इसी समय कविता–कहानी और नाटक के रूप बदलने शुरू हो गए। नाटक लोगों के पास जाने लगा। फैक्ट्री, खेत–खलिहानों में नाटक होने लगा। लगभग दो दर्जन नुक्कड़ नाटक लिखने का मेरा उद्देश्य साफ था, आम दर्शकों से जुड़कर उनसे संवाद करना। आज भी अधिकतर प्रेक्षागृह सरकारी नियंत्रण में हैं और ये संभव नहीं है कि वहां शासन–प्रशासन के खिलाफ कोई नाटक करें। अगर नाटक सीधे प्रशासन पर केंद्रित न भी हो, अगर आप किसी धांधली, कदाचार, बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल उठाएंगे तो अंततः निशाना तो सत्ता पर ही लगेगा। ऐसे में सरकार के लिए आसान नहीं होता है किसी भी व्यवस्था विरोधी रंगकर्मियों के लिए ऑडिटोरियम मुहय्या कराना। ऐसी स्थिति में किसी भी रंगकर्मी के लिए जनता की तरफ मुखातिब होना ही सही कदम होगा। और देखे तो वो सबसे सही समय था अपनी बात को पुरअसर ढंग से लोगों के बीच रखने का। उनदिनों लोग घरों से बाहर निकल रहे थे। जुलूस निकाल रहे थे। हर जोर–जुल्म का विरोध कर रहे थे। नुक्कड़ों पर नाटक ले कर आने जा एक कारण ये भी था कि उनदिनों बंद, घिरे चहारदीवारी के अंदर जो नाटक होते थे, वे समाज से कटे होते थे। अधिकतर नाटक व्यक्तिनिष्ठ, आत्मकेंद्रित होते थे। सत्ता के प्रति सहानुभूति प्रकट करने वाले होते थे। नुक्कड़ नाटक तमाम जड़ता को तोड़ने वाला माध्यम है। कह सकते हैं कि उस समय का सबसे क्रांतिकारी नाट्यरूप था। शायद यही कारण था कि मैं नुक्कड़ों पर उतरा। नुक्कड़ नाटक लिखने और करने का निर्णय लिया।
‘हमें बोलने दो’ और ‘जनतंत्र के मुर्गे’ जैसे नुक्कड़ नाटक की विषयवस्तु संक्षेप में साझा करें और बताएं कि इन नाटकों के लिखने के पीछे आपकी क्या सोच रही ?
बिहार में जब जगन्नाथ मिश्रा की सरकार थी तब एक प्रेस विधेयक पारित किया गया था जिसके अंतर्गत अगर कोई पत्रकार सरकार के विरोध में लिखता है, कोई बोलता है तो उसे सजा स्वरूप जेल जाना होगा। यहाँ तक कि सरकार विरोधी कोई समाचार पत्र किसी के पास से बरामद हुआ तो वो भी सजा योग्य माना जाएगा। इसी ‘काला विधेयक’ के विरोध में मैंने ‘हमें बोलने दो’ नाटक लिखा था और पूरे प्रदेश में घूम -घूम कर नुक्कड़ मंचन किया था। सत्ता विरोधी नाटक होने के कारण प्रशासन द्वारा इसके मंचन को अनेकों बार रोकने का प्रयास किया गया । इंटेलिजेंस द्वारा कलाकारों को धमकाने की कोशिश की गई थी। पर इसके मंचन को जनता का इतना प्रबल समर्थन मिला कि अंततः इस बिल को सरकार द्वारा वापस लेना पड़ा था। ‘जनतंत्र के मुर्गे’ संसदीय कार्य पद्धति पर एक व्यंग्यात्मक नुक्कड़ नाटक है। जैसे सामन्त काल में मुर्गे लड़ाने का चलन था, लोग मुर्गे लड़ाते थे, उसी तरह संसद में हमारे नेता जिस तरह लड़ते हैं उसे देख कर लगता है कि ये जनता की वास्तविक लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत कुछ और होता है। देखने में असली लड़ाई का आभास देता है पर होती है नकली लड़ाई। जनता को भरमाने और बरगलाने के लिए पार्लियामेंट में हमारे प्रतिनिधियों द्वारा ऐसे खेल अक्सर खेले जाते हैं। मेरे नुक्कड़ नाटक अगर सामाजिक होते थे तो राजनीतिक भी। हर नाटक राजनीतिक होता है। उसकी अपनी एक राजनीति होती है। जो नाटक में तटस्थता की बात करते हैं, समझिये वो उतनी ही बड़ी राजनीति कर रहा है। वह अगर जनता की राजनीति नहीं कर रहा है तो व्यवस्था के प्रति सहानुभूति रख रहा है। और ऐसे लोग अंततः सत्ता के पक्ष में ही चले जाते हैं। नुक्कड़ नाटक एक ऐसी विधा है कि अगर आप जनता के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप बहुत दिनों तक प्रगतिशील या जनवादी चेहरे के साथ नहीं रह सकते हैं। एक न एक दिन आप एक्सपोज़ हो जाएंगे।

आपका एक पूर्णकालिक नाटक है ‘अम्बेडकर और गांधी’। इस नाटक के बारे में संक्षेप में कुछ बताएं ?
वर्ण व्यवस्था को लेकर गांधी और अम्बेडकर की क्या अवधारणा है, यह नाटक उस विषय पर केंद्रित है। आज भी वर्ग पर लोग जितना स्पष्ट रूप से बोलते हैं, वर्ण पर बोलने से सकुचाते हैं। गांधी और अम्बेडकर अपने जीवन में लगभग चार–पांच बार मिले थे। गोल मेज कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट, धर्मान्तरण के मुद्दों पर। अम्बेडकर क्लासलेस–कास्टलेस समाज चाहते थे लेकिन गांधी वर्ण व्यवस्था के समूल विनाश के पक्ष में नहीं थे। अस्पृश्यता व भेद भाव तो मिटाना चाहते थे लेकिन वर्ण व्यवस्था को सामाजिक स्थिरता के लिए आवश्यक मानते थे। आज भी उस अवधारणा को मानने वालों की कमी नहीं है। जो उच्चवर्णीय है या वर्ण में विश्वास करते हैं, वे वर्ण व्यवस्था को बनाये रखने की असंख्य दलीलें देते रहते हैं। और यह एक सच्चाई है कि जब तक वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व रहेगा, समाज में असमानता, गैर बराबरी बनी रहेगी। पूरा नाटक इसी विमर्श पर है। संवादों के माध्यम से गांधी और अम्बेडकर के तर्क–वितर्क को रखा गया है। इस नाटक में संवादों की बहुलता है, लेकिन संवादों में नाटकीयता और संवेदना के कारण गति बनाये रखती है। इस नाटक को अस्मिता थिएटर ग्रुप ने देश भर में कई मंचन किये हैं। आज भी इसके शो होते हैं तो देखने के लिए दर्शकों की बड़ी संख्या उमड़ती हैं। शायद इसका एक कारण ये भी हो कि वर्ण–जाति हजारों साल के बाद आज भी जिंदा है। लोग खत्म करना चाहते हैं लेकिन जाति ऐसी चीज है कि जाने का नाम ही नहीं लेती है।
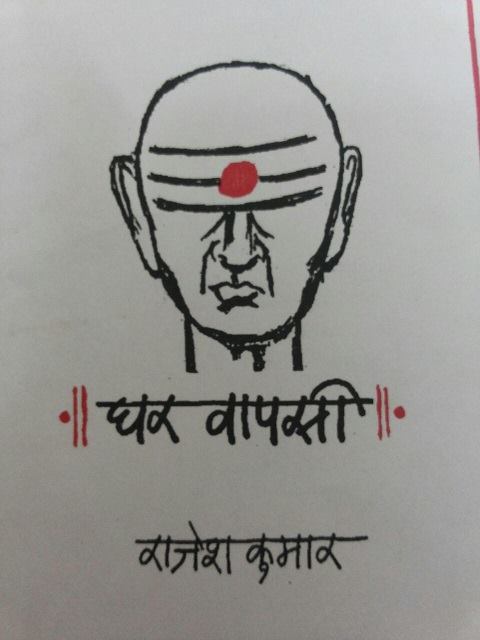
आपके नाटक ‘घर वापसी’, ‘ श्राद्ध’, ‘ तफ़्तीश, ‘ मार पराजय’ और ‘सुखिया मर गया भूख से’ समाज के अंतर्विरोध और मन के अंतर्द्वंदों को दर्शाते हैं। समतामूलक समाज के निर्माण में आप नाटकों की क्या भूमिका देखते हैं ?
साहित्य का समाज में गहरा असर पड़ता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अगर असर नहीं पड़ता तो आये दिन किसी नाटक, सिनेमा को लेकर जो विवाद होता है, न होता। साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं होता है, मशाल भी होता है। चारों तरफ जब अंधेरा छाया होता है, आगे कुछ भी नहीं दिखता है तब मशाल की जरूरत पड़ती है। नाटक केवल यथास्थिति ही दर्शकों के सामने नहीं रखता है, जरूरत पड़ने पर रास्ता दिखाने का भी काम करता है। आज भी कुछ लोगों का मत है कि रास्ता दिखाने का काम नाटक का नहीं है। हम कोई राजनीतिक या उपदेशक नहीं है कि लोगों को मार्ग प्रशस्त करें। इस तर्क की ओट में महानगरों के रंगकर्मी या कह सकते हैं सरकारी संस्थानों द्वारा पोषित–पुष्पित रंगमंच के मुख्य धारा के लोग समाज के उपेक्षित, वर्ण के आधार पर निम्न जाति के लोगों के यथार्थ से टकराने से बचने की कोशिश करते हैं।
वर्ण–जाति के नाम पर जो शोषण होता है, भेद भाव किया जाता है, इन विषयों पर आज भी बहुत कम नाटक लिखे और किये जा रहे हैं। जो लिखे भी गए हैं, संख्या में बहुत कम हैं। अब तक मैंने आठ पूर्णकालिक नाटक लिखे हैं जो किसी न किसी रूप में समाज में व्याप्त अंतर्विरोधों को उठाया है। किसी राजनीतिक दल के दवाब में नहीं लिखा है। जो भी लिखा है, उसका संबंध–रिश्ता समाज से रहा है। ‘घर वापसी’ नाटक में धर्मान्तरण के बाद जाति देने के सवाल को उठाया गया है। आज भी धर्मान्तरण करने वाली संस्थाओं के पास इस बात का जवाब नहीं है कि जाति का आवंटन किस आधार पर हो ? आज इस तरह के नाटक देखने वालों के बीच सकारात्मक असर छोड़ रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व हिंदी रंगमंच में ‘दलित थिएटर’ की चर्चा करने पर अधिकांश रंगकर्मी प्रतिक्रियात्मक भूमिका में आ जाते थे। दलित रंगमंच भी एक धारा है, इसे कोई स्वीकारने को तैयार ही नहीं होता था। सीधा खारिज कर देता था। आज इसे स्वीकृति मिलने लगी है। कई नाटककारों के नाटक इस विषय पर पढ़ने को मिलते हैं। इस पर कई संस्थानों में शोध कार्य हो रहे हैं। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं आया है। लगातार जो नाटक लिखे जा रहे हैं, और नाट्य संस्थओं द्वारा जो किये जा रहे हैं, उसी का परिणाम है। भारतीय रंगमंच का इतिहास वर्ग संघर्षों का ही नहीं, वर्ण संघर्षों का भी है।
आपने प्रेमचंद की ‘सवा सेर गेहूं, ‘ सदगति’, ‘ पूस की रात’ और ‘ कफ़न’ जैसी कहानियों का नुक्कड़ नाट्य रूपांतरण किया है। इसके पीछे क्या वजह रही ?
मुझे प्रेमचंद ने प्रारंभ से ही प्रभावित किया है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि समाज को देखने में प्रेमचंद, भगत सिंह और अम्बेडकर के साहित्य ने बहुत बड़ी मदद की है। मार्क्स ने समाज को तर्क और विज्ञान के आधार पर देखने का नजरिया दिया तो अम्बेडकर के साहित्य ने यथार्थ की पडताल करने का सामाजिक दृष्टि। दक्षिणपंथी साहित्य और साहित्यकारों ने कभी भी प्रभावित नहीं किया। प्रेमचंद जिस तरह से सामाजिक यथार्थ को कहानियों में उठाते थे, मुझे नाटक में उतारने के लिए सदा विवश करता था। शायद यही एक कारण हो नाट्य रूपांतरण करने का।
हाल ही में मैंने आपका एक लेख पढ़ा, जिसका शीर्षक था, ‘ सरकारी मंच पर ‘बाबा साहेब’ का ग्रहण या अधिग्रहण’। आम आदमी पार्टी भगत सिंह और बाबा साहेब का फोटो सरकारी कार्यालयों में लगाने की बात कहती है। दिल्ली और पंजाब में भगत सिंह और अम्बेडकर का फोटो लगाने से क्या समाज में व्याप्त असमानता मिट जाएगी ? आप क्या सोचते हैं ?
कभी वो वक्त था कि भगत सिंह और अम्बेडकर की राजनीतिक पार्टियां आलोचना करने से जरा भी नही चूकती थी। जब भगत सिंह अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे तो विरोधी विचारधारा के लोग उन्हें ‘सिरफिरा’, ‘भटके हुए लोग’ कहने से नहीं चूकते थे। अम्बेडकर के लिए तो कभी पॉजिटिव रिमार्क्स दिए ही नहीं। स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखा तो अम्बेडकर के लिये चार लाइन देना भी भारी लग रहा था। एक वो दिन था और एक आज का है। वर्तमान में हर राजनीतिक दल भगत सिंह और अम्बेडकर को गले लगाने को आतुर है। उनके प्रेम को देख कर किसी को भी भरम हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन दलों का प्रेम एक दिखावा है। वे भगत सिंह और अम्बेडकर को उतना ही स्वीकारते है, जहां तक कोई खतरा न हो। उन्हें इनके विचारधारा से कोई लेना–देना नहीं है। भगत सिंह धर्म को खारिज कर खुद को नास्तिक घोषित करने के संदर्भ में जिस तरह के तर्क देते हैं, ये कभी भी आम आदमी पार्टी और भाजपा को स्वीकार्य नही हो सकता है। जिस तरह अम्बेडकर जात–पात, छूआ–छूत, अस्पृश्यता के लिए वर्ण व्यवस्था को दोषी करार देते है क्या उन्हें सहन होगा ? अम्बेडकर तो वर्ण व्यवस्था को खत्म करने की वकालत करते हैं, क्या इन पार्टियों को यह निर्णय गले के नीचे उतर पायेगा ? ये पार्टियां इनके बहाने वोट बटोर कर सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचना चाहती हैं। लेकिन वे नहीं जानते हैं कि भगत सिंह और अम्बेडकर की विचारधारा पचाना इतना आसान नहीं है। इनके विचारधारा की सान इतनी तेज है कि उनकी आंधी में उड़ कर इतिहास के कूड़ेदान में इस कदर समा जाएंगे कि शायद ढूंढने पर भी मिलना सम्भव न हो।
(साक्षात्कारकर्ता सफाई कर्मचारी आंदोलन से जुड़े हैं।)