प्रख्यात इतिहासकार हरबंस मुखिया बताते हैं कि सिर्फ असंतोष को ही नहीं, बल्कि भारत में कैसे विविधताओ को मौजूदा राजनीति द्वारा हाशिए पर डाला जा रहा हैं। विविधता के आग्रह को अक्सर भारतीय इतिहास को जानने वाले भी पक्का मान लेते है। हालांकि, मुखिया का है कि एक बार नाफ़र्मानी को हाशिये पर डाल दिया गया, तो यह सामाजिक जीवन में चर्चा को बंद कर सकता है ।
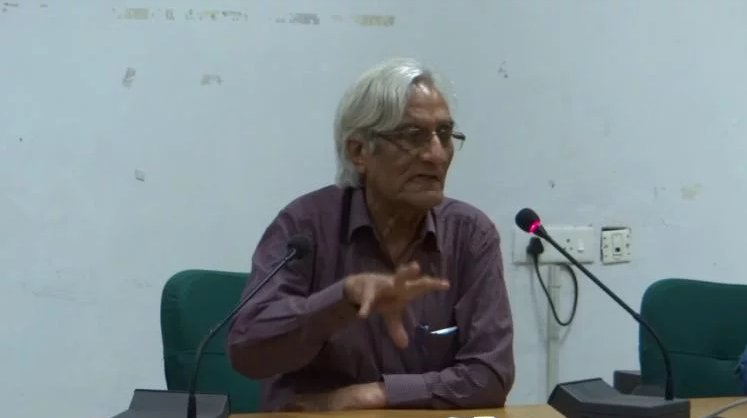
हरबंस मुखिया, छवि पाठ्यक्रम: यूट्यूब
भारतीय जनता पार्टी अपने 'न्यू इंडिया ’के विचार के बारे में बात करती है। यह भारत उस भारत से अलग कैसे है जिसका आपने एक इतिहासकार के रूप में अध्ययन किया है?
6वीं शताब्दी में, ग्रीक दार्शनिक हेराक्लीटस ने बदलाव का वर्णन करने के लिए एक काव्य वाक्यांश का उपयोग किया था कि – ‘ केवल बदलाव ही सनातन है'। यह बदलाव हमेशा राज्य और समाज के बीच बातचीत के जरीए होता है। राज्य अक्सर धर्म, आर्थिक संरचनाओं और सामाजिक संबंधों में बदलाव का प्रमुख प्रस्तावक होता है। तीसरी शताब्दी में अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, प्रारंभिक रोमन धर्मशास्त्री और सम्राट, ऑगस्टीन और कॉन्स्टेंटाइन ने, ईसाई धर्म का प्रसार किया। राज्य संरक्षण के माध्यम से ही समाज में इस्लाम और हिंदू धर्म प्रमुख हो गए थे।
लेकिन समाज भी बदलाव के कुछ मापदंड तय करता है, उदाहरण के लिए, यह सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से अपने मापदंड तय करता है। इसलिए, बौद्ध धर्म राज्य सत्ता के माध्यम से अस्तित्व में नहीं आया था। बुद्ध, हालांकि खुद एक राजा था, लेकिन वह एक व्यक्ति के रूप में बौद्ध दृष्टिकोण पर पहुंचे। इस्लाम को भी लोगों द्वारा फैलाया गया था। इसलिए, समाज, राज्य के लिए एजेंडा तैयार करता है। आज, राज्य और समाज के बीच की यह अंतरंगता या संबंध भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बद्स्तुर जारी है। 20 वीं और 21 वीं शताब्दियों में राज्य और समाज की परिभाषित विशेषता-लोकतंत्र और चुनाव आदि रहा है, जो आज़ बदल रहा है। आज, राज्य सत्ता की कार्रवाई ने लोकतंत्र को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। हर जगह चुनाव जोड़ तोड़ का मसला बन गया हैं। पैसे और बाहुबल की जोड़तोड़ के अलावा, एजेंडे में हेरफेर भी शामिल है।
इस हेरफेर के परिणाम क्या है?
अंतर यह है कि अब राज्य एजेंडा तय कर रहा है, चाहे वह संयुक्त राज्य अमेरिका हो, तुर्की हो या फिर भारत हो। इस एजेंडे के माध्यम से, राज्य को समाज की ऐसी प्रतिक्रिया मिलती है जिसे उसने पहले से ही व्यवस्थित किया हुआ है। परिणाम वही होते हैं जिन्हे राज्य ने पहले ही तय किया हुआ हैं। चुनाव केवल प्रबंधन का मामला बन गए हैं, लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व अब चुनाव नहीं करते हैं बल्कि वे इसका अर्थ खो रहे हैं।
क्या यह विरोध या असंतोष की स्पष्ट आवाज़ की कमी के कारण है?
सैद्धांतिक रूप से असंतोष लोकतंत्र का एक हिस्सा है। राज्य को विरोधी आवाज़ की जरूरत होती है, विचारों में कुछ विचलन होते रहना चाहिए वरना यह बहुत जल्दी ढह जाएगा। स्टालिन के मरने के ठीक बाद राज्य ध्वस्त हो गया था। हिटलर का राज्य उन्ही के जीवनकाल में ढह गया। इसलिए, राज्य हमेशा उन आवाजों को अनुमति देता है,जो कुछ असंतोष व्यक्त करते है मगर जो यथास्थिति को चुनौती नहीं देते हैं। लेकिन आज जो परिवर्तन हो रहा है, उसमें वे राज्य शक्ति का समर्थन कर रहे हैं न कि असंतोष का।
इसके विपरीत प्रतिक्रिया क्यों उत्पन्न नहीं हो रही है, यदि राज्य मजबूत हो रहा है, तो उसके अनुपात में असंतोष क्यों नहीं बढ़ रहा है?
इसका मुख्य कारण अनेक संस्थानों, विशेषकर मीडिया पर राज्य नियंत्रण है। ऐसे दर्शकों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है, जो मीडिया में जो कुछ भी देखते हैं उसकी आलोचना करते हों। आलोचना करने के लिए मीडिया को ज्ञान के विशाल भंडार की आवश्यकता होती है, जिसे शिक्षित लोगों के लिए भी हासिल करना आसान नहीं है। राज्य, समाज, सभ्यता या धर्म की आलोचना करना वैसे भी बहुत कठिन है। लेकिन हर जगह धर्मों का आलोचनात्मक होना ज़रूरी है। आज, विविधता के बड़े स्थान को हिंदू धर्म में कुचल दिया जा रहा है। जैसे-जैसे राज्य ताकतवर होता जा रहा है, वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय एजेंडा खुद तय कर रहा है।
एजेंडे को क्या परिभाषित करता है?
19 वीं शताब्दी में, राष्ट्र-राज्य का नारा बुलंद किया गया था और यूरोप के देश युद्ध में चले गए। फिर वैश्वीकरण का नारा आया और इसने राष्ट्रीय सीमाओं को काट दिया और आर्थिक बाधाओं को तोड़ दिया। आज, हम फिर से राष्ट्र के विचार और उस पर एक बंद राष्ट्र के विचार पर वापस आ गए हैं। ब्रिटिश सरकार यह तय नहीं कर सकती है कि उसे यूरोपीय संघ का हिस्सा बनना चाहिए, अमेरिका इमीग्रेशन के संकट से जुझ रहा है। भारत और तुर्की जैसे देशों में भी सोशल मीडिया के संदेशों की बमबारी है।
सोशल मीडिया एक बहुत ही लोकतांत्रिक घटना है, लेकिन इसने पूरी तरह से बेतुके विचारों और गाली के लिए जगह खोल दी है। इसका विनाशकारी प्रभाव यह है कि सोशल मीडिया संगठित हस्तक्षेपों की एक व्यवस्था बन गई है। एक व्यक्ति की राय, यहां तक कि उसके द्वारा दी गाई गाली या दुरुपयोग, विचारों की विविधता में उसमें जोड़ देता है। विशेष रूप से भारत में, सोशल मीडिया का संगठित हस्तक्षेप इतना एकतरफा है कि यह विविधता को मार रहा है। इसलिए, यह लोकतांत्रिक पहुंच का बहुत बड़ा विरोधी थिसिस बन गया है।
इसलिए, यह केवल असंतोष पर हमला नहीं है बल्कि विविधता पर भी है?
हां, भारत में जो हो रहा है वह विविधता को तबाह करने की कोशिश है। आप आर [प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी] के खिलाफ एक भी शब्द कहते हैं तो आपको 'राष्ट्र-विरोधी' कहा जाता है। हिंदू विरोधी देशद्रोही का समीकरण बन रहा है और वह बिक रहा है। उदाहरण के लिए, लोगों ने स्वीकार किया कि जेएनयू (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय) ‘राष्ट्र-विरोधी ’है।
क्या भारत की विविधता इसे एक निश्चित दुरी तक जाने से रोकेगी?
यह हमारी एक अलग राय है, कि भारत की विविधता एक दृष्टिकोण को अन्य सभी विचारों पर हावी नहीं होने देगी। वास्तव में, भारत ने अपने इतिहास के माध्यम से अपनी विविधता को विकसित किया है। लिखित इतिहास के पहले के समय के दिनों से,जबरदस्त संख्या में विभिन्न समुदाय/समूह भारत में आए इसने कई आक्रमणों का भी सामना किया। यह कोई अनोखी बात नहीं है। दुनिया के हर इंच ने माइग्रेशन देखा है यहां तक कि आइसलैंड, और न्यूफ़ाउंडलैंड तक ने ये माइग्रेशन देखा है जो ग्रह पर सबसे दूर और ठंडे क्षेत्र है। और यह भी सत्य है कि सारी मानवता एक मिश्रित नस्ल है।
इसलिए, यह कहना असंभव है कि यहां का कौन और बाहरी व्यक्ति कौन है?
कोई अंदर का या बाहरी व्यक्ति नहीं है। इस विचार को पूरी तरह से रचा गया है। केवल 18 वीं और 19 वीं शताब्दी में विकसित राष्ट्र की अवधारणा पासपोर्ट के आधार पर अंदरूनी और बाहरी लोगों को परिभाषित करती है। ब्रिटिश पासपोर्ट रखने पर आप ब्रिटेन के अंदरूनी व्यक्ति हो जाते हैं, या फिर आप एक बाहरी व्यक्ति हैं। यह बेहद आसान था। पहले भी, सैन्य कार्रवाई ने सीमाओं का बचाव किया था, लेकिन ये राष्ट्रों की सीमा नहीं बल्कि साम्राज्य थे।
क्या राष्ट्र की धारणा के बारे में हमारे अतीत की तुलना में आज क्या बात अलग हैं?
वे मौलिक रूप से अलग धारणाएँ हैं। प्रत्येक साम्राज्य या राज्य के लिए, भव्यता के जरीए अपनेपन की भावना को पैदा करना एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था। अशोक साम्राज्य का विचार ’महान’ होना था, कि वह बड़े पैमाने पर ‘आम लोगों’ का राज्य था जो अपनेपन का एहसास दिलाता था। महानता और भव्यता की यह धारणा अतीत में भी विद्यमान थी, जैसा कि आज है। इसलिए, हम कहते हैं कि 'भारत एक महान देश है' और इसलिए 'मुझे भारतीय होने पर गर्व है'।
हम यह भी सुनते हैं कि 'हिंदू धर्म एक महान धर्म है' और इसलिए गर्व से कहो हम हिंदू हैं - गर्व के साथ कहो कि तुम हिंदू हो। सांस्कृतिक भव्यता अपनेपन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। मुगल शब्द आज भी भव्यता के बराबर है। हम विजय माल्या को 'मुगल शराबवाला' कहते हैं और 'मुगल फिल्म’ का इस्तेमाल करते हैं। मुगल शब्द का अर्थ है कि जब आप ताजमहल को देखते हैं, तो आप यह कहते हुए गर्व महसूस करें कि यह मेरा देश है और यह स्मारक मेरा है।
लेकिन भव्य निर्माण का युग समाप्त हो चुका है।
स्मारकों की भव्यता ही नहीं बल्कि मूल्य भी बदल गए हैं। अतीत में, साम्राज्यों या राष्ट्रों के क्षेत्र लगातार विस्तारित होते थे और अनुबंधित थे। विस्तार भव्यता की भावना पैदा करता था और इसलिए एक साम्राज्य के वहां का मूल होने या बाहरी होने के मूल्य को परिभाषित करता था। आज, राष्ट्र राज्यों के पास मौजूद प्रदेश कमोबेश जमे हुए हैं। इसलिए, आप अपनी अर्थव्यवस्था के बजाय भव्यता को प्रोजेक्ट करते हैं। आप दावा करते हैं कि आप एक महान आर्थिक शक्ति हैं या अपनी संस्कृति की महिमा के बारे में बात करते हैं।
हमारे देश ने भव्यता को धर्म के क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया है। हम हिंदू धर्म की महिमा का निर्माण कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में एक 'अन्य' भी बना रहे हैं। इसलिए, यदि आप 'गर्वित हिंदू' नहीं हैं तो आप 'अन्य' हैं। या आप 'हिंदू विरोधी' हैं और इसलिए, 'राष्ट्र विरोधी' हैं। यूएस की भव्यता आर्थिक भव्यता, इसकी सैन्य शक्ति, अपने क्षेत्र की विशालता और दुनिया भर में प्रभाव है। इन बातों का भारत स्पष्ट रूप से दावा नहीं कर सकता है और इसलिए, वह धर्म और संस्कृति की भव्यता का दावा करता है। हम इसे पुरानी सभ्यता जैसे शब्दों में व्यक्त करते हैं।
क्या, संस्कृति की भव्यता के बारे में बात करना गलत है?
किसी भी प्रकार की भव्यता को हमेशा अपनेपन की भावना का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि [हिंदू भगवान] गणेश प्लास्टिक सर्जरी से बने हैं। इस तरह के बेहुदगी भरी बातें विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों [द्वारा] भी थोपी जा रही है। जिस संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है वह ताजमहल, स्मारकों और लघु चित्रों की संस्कृति नहीं है बल्कि धर्म की संस्कृति है। यह विचार कि हिंदू धर्म एक महान धर्म है, प्रचारित किया जा रहा है लेकिन इसकी महानता का कोई विशिष्ट चित्रण करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है।
एक तरफ प्लास्टिक सर्जरी की बात, फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स के संदर्भ में भव्यता की धारणा या जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को निरस्त करना, किस तरह के समावेश को प्रतिबिंबित करता हैं?
वर्तमान में हमारी भव्यता समावेशी नहीं है, लेकिन मौलिक आधार के रूप में विशिष्ट है। यह एक ऐसी दृष्टि है जो कहती है कि यदि आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप हमारे खिलाफ हैं। यह भव्यता की एक बहुत अलग परिभाषा है। इससे पहले हम एक वाक्यांश सुनते थे कि ‘ साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डुबता है’। उस साम्राज्य की भव्यता समावेशी थी। उपनिवेशों में, साम्राज्य के पास, ‘अन्य’ थे, लेकिन उपनिवेशों के रूप में वे साम्राज्य का हिस्सा थे। अमेरिका अब इमिग्रेशन के बारे में चिंतित है लेकिन इसकी भव्यता बहिष्कार के आधार पर विकसित नहीं हुई। बल्कि यह विभिन्न लोगों का इसमें हुआ समावेश था जिन्होंने इसकी भव्यता का निर्माण किया। आज भारत में जिस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है वह यह है कि यदि आप हिंदू नहीं हैं तो आप इसकी भव्यता से संबंधित नहीं हैं; आप न केवल संस्कृति बल्कि क्षेत्र के लिए भी एक बाहरी व्यक्ति हैं। यही कारण है कि आप अक्सर सुनते हैं कि ‘भारत से बाहर जाओ’।
यदि साम्राज्य और राष्ट्र एक जैसी भव्यता को बढ़ावा देते हैं, तो क्या आप अतीत से राजनीतिक जीवन की तुलना कर सकते हैं कि यह अब कैसा है?
इतने लंबे समय तक जीवित रहने का लाभ यही है, कि आप इतने सारी घटनाओं के साक्षी हो जाते हैं। 1967 में हुए एक अद्भुत बदलाव ने भारत को पीछे छोड़ दिया। पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर जगह कांग्रेस पार्टी राज्य का चुनाव हार गई थी। इससे हमें बदलाव की बहुत उम्मीद थी क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस चुनाव हार गई थी, हालांकि इसने केंद्र में सरकार को बनाए रखा।
उस समय बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश था ...
जी हां, उस समय, दिल्ली के कनॉट प्लेस [अब राजीव चौक] में इंडिया कॉफ़ी हाउस में एक कप कॉफ़ी, चार आना की कीमत हुआ करती थी। हर शाम बुद्धिजीवी वर्ग - जिसका बुद्धि और गरीबी दोनो पर एकाधिकार था - कॉफी पीने के लिए वहां इकट्ठा होता था। अचानक, उनकी कॉफी की कीमत में एक या दो आना की वृद्धि हो गई। इसके खिलाफ वहां कॉफी हाउस में किसी ने प्राइस राइज रेजिस्टेंस मूवमेंट बनाया। किसी तरह यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। किसी को भी इसका पता नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि कैसे इस कॉफी शॉप से, हर जगह एक सामाजिक अशांति सी पैदा हो गई थी। निश्चित रूप से, यह पूरे उत्तर भारत में फैल गया, लेकिन जैसे-जैसे यह पूर्व और पश्चिम में गया, इसने हर जगह कांग्रेस सरकारों को गिरा दिया।
विशेष रूप से वामपंथियों के लिए, इस आंदोलन ने आशा पैदा की कि चीजें बदलने जा रही हैं। प्रोफेसर रणधीर सिंह और बिपिन चंद्र और मैं, हालांकि मैं काफी छोटा था, सभी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। हम उस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) में थे। हमने पंजाब के गाँवों में जाना शुरू किया और जो कुछ होने जा रहा है उसके बारे में जागरूकता पैदा की। इन यात्राओं में से एक में हमारे साथ महान पंजाबी कवि [अवतार सिंह] पाश भी आए थे। मुझे याद नहीं है कि उन्होंने कौन सी कविता का पाठ किया था लेकिन मुझे उस सत्र में किसी अन्य कवि की एक पंक्ति याद है। ‘ओय क्रांति तू औदी क्यूं नै’ - हे, क्रांति! तुम आती क्यों नहीं हो? '' इस तरह हम सब क्रांति के लिए बेताब थे। लेकिन हम उस समय बचकाना थे। बहुत जल्द, यह प्रणाली पुनः जिवित हो गई और अगले चुनावों ने इंदिरा गांधी भारी बहुमत से वापस आ गाई। क्रांति छिन्न-भिन्न हो गई लेकिन 1967 ने हमें उम्मीद दी कि चीजें बदल सकती हैं, हालांकि वे उस समय नहीं बदली।
तो अतीत और अब के बीच का अंतर उम्मीद है।
आजादी के बाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने भाषणों के जरीए बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाई थी। अपनी टूटी-फुटी हिंदी में उन्होंने आर्थिक आत्मनिर्भरता, संसदीय लोकतंत्र, योजना आदि की बात की थी। भव्यता की धारणा पर वापस आते हुए, नेहरू, [गमाल अब्देल] मिस्र के नासिर और [जोसिप ब्रोज़] यूगोस्लाविया के टीटो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तीन निर्माता थे। वे विश्व नेता माने जाते थे क्योंकि वे अमेरिका या यूएसएसआर के खिलाफ या कम से कम उनके बीच खड़े हो जाते थे।
इससे हमें गर्व की अनुभूति हुई थी। इसने नेहरू के दृष्टिकोण को बहुत मंत्रमुग्ध बना दिया था। नेहरू आज ज्यादा बदनाम हैं, लेकिन आपको उनकी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पढ़ना चाहिए, यह महसूस करने के लिए कि उन्होंने हिंदू संस्कृति की कितनी गहराई से सराहना की है। उन्होंने इसे एक तरह से समझा कि मोदी या [गृह मंत्री अमित शाह या पूर्व डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी] नहीं समझ पाए। एकमात्र हिंदू धर्म वे जानते हैं जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से है और वह हिंदू धर्म समरूपता वाला धर्म है। यही वह है जो हिंदुत्व है - दूसरों पर दादागिरी। और इस हिंदुत्व में 'अन्य' का अर्थ है मुसलमान।
आप इस बदलाव को कैसे चित्रित करेंगे?
अन्य अंतर यह था कि असंतोष या विरोध के लिए बड़ा स्थान था। एक बार, मैंने और मेरे एक सहयोगी ने रेडियो चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने भारत की प्रगति के बारे में बात की और मैंने, एक पुराने समय के मार्क्सवादी होने के नाते, इस बारे में बात की कि यह सिस्टम कैसे काम नहीं कर रहा है - दोनों तरफ न बदलने वाले विचार थे (हंसते हुए)। बाद में, मेरे सहयोगी ने कहा कि मैं सिस्टम के खिलाफ बोलने के मामले में बहुत बोल्ड हूं।
मुझे याद है कि मुझे उसे यह बताना पड़ा कि सिस्टम का विनाश करना भी सिस्टम का ही एक हिस्सा है। इसलिए, हम उस समय कह सकते थे कि यह व्यवस्था बहुत अधिक भ्रष्ट है, इसलिए यह नहीं चलेगी ... और ठीक ऐसा ही हुआ। सत्तर के दशक के उत्तरार्ध में इंदिरा गांधी असंतोष का दमन करने की नींव रखी। उसने संस्थागत वित्तीय भ्रष्टाचार की नींव भी रखी। खुद के लिए नहीं बल्कि अपनी पार्टी के लिए, और तब से यही सब चल रहा है। अब भ्रष्टाचार इतना संस्थागत है कि आप इस पर सवाल भी नहीं उठा सकते हैं। एक विधेयक को हाल ही में लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था जिसमें राजनीतिक दलों के योगदान के बारे में सवाल पूछने से भी मना कर दिया गया है।
तो हम विरोध या असंतोष को नकारने के लिए और नीचे गिर गए हैं?
इंदिरा गांधी ने पहला कदम उठाया था लेकिन अब हम आलोचना करने की किसी भी स्वतंत्रता से इनकार करना चाहते हैं। जो लोग किसी भी तरह की आलोचना को नहीं सुनना चाहते हैं वे हमेशा कहते हैं कि आपको आलोचना करने की सभी स्वतंत्रता है- लेकिन''। ‘लेकिन' हमेशा जुड़ा रहता है और इसका मतलब है कि' हम आपको बताएंगे कि हम कितनी आलोचना कर सकते हैं'। मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे समाज के साथ क्या किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था नीचे जाती है तो वह ठीक हो सकती है, लेकिन समाज नीचे जाता है तो वह ठीक नहीं हो सकता है।
समाज क्यों नहीं उबर सकता है?
इतिहास में वापस जाओ।
बंटवारे की तरफ?
बंटवारा हाँ, लेकिन उससे परे। भारत बंटवारे से बहुत जल्दी उबर गया।
कुछ लोग कहते हैं कि हम अभी भी बंटवारे से उबर नहीं पाए हैं।
एक तरह से हाँ, बंटवारे ने दरार डाल दी और यही कारण है कि हम अभी भी 'पाकिस्तान जाओ' का नारा सुनते हैं। फिर भी तथ्य यह है कि इस्लाम पहले भारत में आया और बाद में मुस्लिम राजा आए। इस्लाम ने समाज को बदला था - मैं बदतर के लिए नहीं कह रहा हूं। इससे पहले बौद्ध धर्म ने समाज को बदला था, फिर गुप्ता काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ था। लेकिन इन बदलावों ने भारत की सभी विविधताओं को खत्म नहीं किया था। इसलिए, यह मान लेना कि विविधता वापस अपने आपको पुनर्स्थापित करेगी ... यह सही है, विविधताएं कभी मरती नहीं हैं। यहां तक कि पाकिस्तान जैसे देश में भी विविधता है। लेकिन एक प्रकार की सामाजिक शक्ति के रूप में विविधताएं इस तरह की एक समरूपता वाली (होमोजेनिक) शक्ति के रूप में हावी हो जाती हैं। विविधता मिटती नहीं है, निश्चित रूप से, लेकिन वे अभिभूत हो जाती हैं और इसलिए, हाशिए पर चली जाती हैं। वह हाशिये पर जीवित रहती हैं। जिस तरह से वह पाकिस्तान में जीवित हैं।
और हाशिये पर पड़ीं विविधताएं कभी भी राज्य के लिए खतरा नहीं बन सकतीं हैं?
यही एक बड़ा बदलाव है जो हुआ है। अर्थात् एक संगठित तरीके से - एक समरूप समाज की स्थापना के लिए और एक विकसित कार्यक्रम का विरोध किया गया। हम एक समरूप पार्टी को देख रहे हैं जो एक समरूप प्रजातंत्र चला रही है जो समरूप आर्थिक नीतियों का अनुसरण कर रही है और इन सबसे ऊपर वे एक समरूप संस्कृति और समाज चाहते हैं। केवल एक तरीके से, मैं लगभग आरएसएस का प्रशंसक बन गया हूं।
सौ साल पहले, 1925 में, इसके संस्थापकों को एक दिन भारत को उनकी दृष्टि के अनुसार बदलते हुए देखने की दृष्टि थी और यह दृष्टि वह है जिसे आज हम देख रहे हैं। उन्होंने समाज को अपनी दृष्टि के हिसाब से ढाल लिया है। हर जगह आरएसएस की शाखाएं हैं। उन्होंने बच्चों के लिए शिशु मंदिर स्कूल स्थापित किए हैं, जहाँ उन्होंने समाज को आरएसएस के विचारों के लिए तैयार किया। अब जो होने की संभावना है वह राजनीतिक शक्ति और सामाजिक संगठन [आरएसएस] का मिलन है। इसलिए, न केवल आरएसएस बल्कि समाज पर इसका प्रभाव फैल जाएगा। राजनीतिक शक्ति और सामाजिक संगठन के बीच यह संगम पहले मौजूद नहीं था। राज्य और समाज के बीच अतीत में चर्चा रहती थी, लेकिन आरएसएस के प्रभुत्व के जरीए इसे खत्म किया जा रहा है।
क्या हम इसे, जैसा कि द न्यू यॉर्क टाइम्स के स्तंभकार ने हाल ही में कहा, दूसरा विभाजन कह सकते हैं?
विभाजन एक क्षेत्रीय अवधारणा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह एक उपयुक्त शब्द है, लेकिन सामाजिक विभाजन के मामले में यहां एक विभाजन नज़र अता है। दिमागों का बंटवारा हो रहा है। आपको एक पक्ष या दूसरे पक्ष क़े साथ होना है। आपको ‘जय श्री राम’ कहना होगा या फिर आपको बाहरी व्यक्ति माना जाएगा। आप नहीं कह सकते कि आप एक हिंदू हैं, लेकिन जय श्री राम’ नहीं कहेंगे और जो भी आपसे मांग की जाती है।
जैसा कि एक इतिहासकार एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण लेता है, भविष्य के लिए आपका दृष्टिकोण क्या है?
अंग्रेजों ने भी भारत में भारी और मूलभूत परिवर्तन किए थे, फिर भी लंबे समय तक उनके प्रभुत्व का क्षरण होने लगा। आज के प्रभुत्व को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, खासकर जब ऐसा करने के लिए रास्ते इतने खुले हैं। मेरी शिकायत विपक्ष से है। 2019 के चुनावों से पहले दीवार पर लिखा हुआ था कि उन्हें एकजुट होना चाहिए था, लेकिन स्थानीय स्तर की क्षुद्रता ने इसे दबा दिया। जबकि अन्य समय में समाजवादियों और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन काम करता था; लेकिन अब इसे 'अविश्वसनीय' मान लिया गया। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गठबंधन सहयोगी को कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनने दिया लेकिन उनकी अपनी पार्टी के [पूर्व मुख्यमंत्री के. सिद्धारमैया इसमें काफी अनिच्छुक दिखे थे। कुल मिलाकर, विपक्ष के पास भारत की विशालता की दॄष्टि नहीं है।
इस सबके परिणामस्वरूप भाजपा मजबूत होती दिख रही है।
उल्लेखनीय रूप से, भाजपा में कोई टूटन नहीं है, जबकि कांग्रेस और अन्य दलों से नेता लोग पार्टी छोड़ रहे है। यहां तक कि भाजपा के आलोचक, जैसे यशवंत सिन्हा, बाहर निकलने के बावजूद किसी अन्य दल में शामिल नहीं हुए हैं। बीजेपी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, जहां दांव बहुत ऊंचे हैं और अन्य दल ऐसी व्यवस्था नहीं बना पाए हैं। जमीनी स्तर पर बदलाव की राजनीतिक चर्चा छेड़ने का कोई विकल्प नहीं है और यही भाजपा और आरएसएस की जीत है।
सत्ता में पार्टी का प्रयास पूरी तरह से चुनावी जीत हासिल करने के लिए नहीं है ...
उनकी दृष्टि हिंदू राष्ट्र की है, यही कारण है कि वे लगातार संविधान के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं, इसे मिटाते हैं, और वे एक तरह से हंसते हुए कहते हैं कि वे इसके साथ किसी भी तरह का हेरफेर कर सकते हैं जैसा वे चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने कश्मीर के मामले में किया है। वे धारा 370 को ’अस्थायी’ प्रावधान कहते हैं – जैसे भी अपनी बात को सही ठहराना है। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है और यह अपने स्वयं के प्रावधानों के भारी हेरफेर और उल्लंघन के लिए भी खुला है। वे यही अभ्यास कर रहे हैं और अपना उल्लु सीधा कर रहे हैं। इसमें अंतिम हार आम लोगों की होगी क्योंकि यदि आप एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जो लगातार तनाव और ‘अन्य’ के नाम काम कर रहा है, तो आप हिंदू होने के बावजूद एक हारे हुए व्यक्ति होंगे। इसलिए मैंने उल्लेख किया कि चीजें बदलती रहती हैं। हमें हेराक्लिटस को नहीं भूलना चाहिए।