बीते कुछ दशकों में महिलाओं के मुद्दों पर बहुत से नए सवाल उठाए गए हैं। समाज में इन सवालों को उठाने में नारीवादी या फ़ेमिनिस्ट महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। लेकिन आज भी नारीवाद या महिलाओं के मुद्दों पर जागरुकता बहुत बड़े तबक़े तक नहीं पहुँच पायी है। लेकिन उसके क्या कारण हैं?
अगर बात सिर्फ़ हमारे देश की ही करें तो बहुत सी महिलाएं आज भी अपने अधिकारों को लेकर जागरुक नहीं हैं और जो हैं उनको हमारा समाज अपना नहीं पाया है या यूं कहें कि समाज का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी महिलाओं को बदलते हुए देखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यह कहना ग़लत नहीं होगा कि महिलाओं के मुद्दों पर एक तबक़ा ऐसा भी है जिसने अपनी रूढ़िवादी सोच को कुछ स्तर तक चुनौती भी दी है।
साल 2018 और 2019 में महिलाओं और जेंडर के विषय पर बहुत सी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुईं। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फ़ैसला दिया और कहा कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाज़त न देना संविधान के अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) का उल्लंघन है। इस फ़ैसले पर जहां एक बड़ा तबक़ा महिलाओं के प्रवेश का विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ताक पर रखते हुए विरोध करने सड़कों पर उतर आया वहीँ एक बहुत छोटा तबक़ा महिलाओं के पक्ष में भी खड़ा नज़र आया। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार पर फ़ैसला देते हुए कहा पति पत्नी का मालिक नहीं होता और ऐसे ही एक और ऐतिहासिक फ़ैसले-377 यानी समलैंगिकता को अपराध ठहराने वाली धारा को असंवैधानिक ठहराने पर भी कुछ लोग समलैंगिक जोड़ों के मुद्दों पर संवेदनशील भी नज़र आए। आज से कुछ साल पहले आप और हम कोर्ट से ऐसी प्रगतिशील बातें सुनने की उम्मीद नहीं कर सकते थे और न ही लोगों के समर्थन की।
#मीटू आंदोलन के तहत बहुत सी महिलाएं कार्यस्थल पर अपने साथ होने वाले यौन शोषण पर खुलकर सामने आईं जिससे इस विषय से भी एक नई बहस छिड़ी। यह साफ़ देखा जा सकता है कि सड़कों से लेकर, विश्वविद्यालयों और कार्यस्थलों और यहाँ तक कि अदालतों तक में महिलाओं के विषय होने वाली बहस में थोड़ा अंतर आया है। यानी अब सभी महिलाओं को सिर्फ़ उनकी पहचान या जेंडर के आधार पर उनके साथ भेदभाव करना उतना आसान नहीं रह गया है जितना आज से 30 साल पहले था।

लेकिन आज भी अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं कई तरह की चुनौतियों का सामना करती हैं। तो सवाल उठता है कि क्या समाज में महिलाओं को लेकर ज़रा भी बदलाव आया है और आया है तो इसके क्या बड़े कारण हैं और जो बदलाव नहीं आया है उसके लिए क्या रास्ते हो सकते हैं?
नारीवाद सिर्फ़ किताबों में पढ़ने-पढ़ाने वाली विचारधारा नहीं है। अकादमिक क्षेत्रों में इसकी शुरुआत महिला आंदोलन से ही हुई है और इसके ज़रिये महिलाओं के उत्पीड़न को ख़त्म करने और ग़ैर बराबरी को चुनौती देने की दिशा में बढ़ना चाहिए।
ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब का दे रहा है एक नया प्रोजेक्ट "फ़ेमिनिस्ट तालीम"। इस प्रोजेक्ट पर दिल्ली के अंबेडकर विश्वविद्यालय और स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के कई शिक्षक और छात्र-छात्राएं काम कर रहीं हैं। "टीचिंग फ़ेमिनिज़्म, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स प्रोजेक्ट" विषय पर दोनों विश्वविद्यालय यूजीसी-यूकेईआरआई (UGC-UKERI) के तहत साथ आकर ऩारीवाद को नए चश्मे से देखने की कोशिश कर रहें है। इसका उद्देश्य लोगों को नारीवाद से जुड़े मुद्दों पर जागरुक करना, क्लासरूम में पढ़ाई जाने वाले नारीवाद के विषयों को अलग-अलग से क्षेत्रों से जोड़ना और उत्तर (यू.के) और दक्षिण (भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देश) में इस विषय पर संवाद को बढ़ाना है।
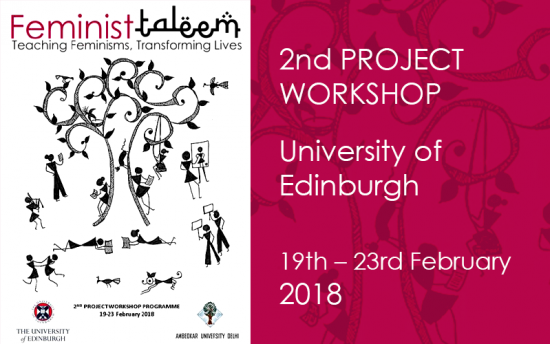
इस प्रोजेक्ट को समझाते हुए अंबेडकर विश्वविद्यालय की जेंडर एंड वूमेन स्टडीज़ विभाग की प्रोफ़ेसर कृष्णा मेनन कहती हैं, "इस प्रोजेक्ट का शीर्षक 'फ़ेमिनिस्ट तालीम' ही इसके उद्देश्य को समझाता है। ये अंग्रेज़ी शब्द फ़ेमिनिस्ट जिसका अर्थ है- नारीवादी और उर्दू /हिन्दुस्तानी शब्द तालीम, जिसका अर्थ है शिक्षा, दोनों को मिलाकर बना है। ये महात्मा गांधी के विचार 'नई तालीम' से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें शिक्षा को सब तक पहुँचाने का और सबको जोड़ने का महत्व भी समझाया गया है। इसके ज़रिये हम नारीवाद के विषय पर एक दूसरे से जानकारी बराबर से साझा करते हैं। ये प्रोजेक्ट इसलिए अलग है क्योंकि इसमें विचार और जानकारी साझा की जाती है न कि पढ़ी-पढ़ाई जाती है। इस प्रोजेक्ट में हम शिक्षक और कई छात्र-छात्राएं एक साथ आकर बराबरी से काम कर रहें हैं। एक दूसरे को सिखा रहें हैं और इसके पीछे के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलग-अलग लोगों से जुड़ने और उनसे संवाद करने के तरीक़ों पर विचार कर रहे हैं।"
प्रो.कृष्णा कहती हैं, "नारीवाद के ज़रिये महिलाओं की ग़ैरबराबरी और महिला उत्पीड़न को कई नए तरीक़ों से देखने में मदद की है। हम आज के समय में इन मुद्दों को और बेहतर समझने समझाने के लिए क्लासरूम का उपयोग कर रहें हैं और इस प्रोजेक्ट के ज़रिये ये जानने की कोशिश कर रहें हैं कि इनसे क्या बदलाव लाए जा सकते हैं।"
यह सच है कि सब महिलाएं कोई 'समान कैटेगरी' की नहीं हैं। अलग-अलग वर्ग, जाति, क्षेत्र से आने वाली महिलाओं के मुद्दे अलग भी हैं पर कहीं न कहीं जुड़े भी हैं। जैसे अगर एक पिछड़े तबक़े से आने वाली मज़दूर महिला की बात करें तो हम देखते हैं कि उसे वर्ग, जाति और पितृसत्ता तीनों के कारण उत्पीड़ित किया जाता है। यह महिला हर तरह से समाज के हाशिये पर खड़ी है। लेकिन उच्च वर्ग और जाति से आने वाली महिलाएं भी पितृसत्ता जैसी व्यवस्था का शिकार होती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो पितृसत्ता एक ऐसी व्यवस्था है जो हर तबक़े और जाति की महिला को अलग-अलग तरह से पीछे धकेलती है और समाज के अन्य पिंजरों में उन्हें क़ैद करती है।

लेकिन यह भी सच है कि उस मज़दूर महिला के बहुत से मुद्दों को हम क्लासरूम में बैठकर नहीं समझ सकते या ठीक वैसे ही नहीं देख सकते जैसे वो अपने नज़रिये से समझती होंगी। उसी तरह किसी मीडिया हाउस या पब्लिशिंग हाउस या अन्य क्षेत्रों में काम करने वाली की चुनौतियों को भी उनके नज़रिये से समझना ज़रूरी है। इसलिए किसी भी तरह की जानकारी को आपस में साझा करना ज़रूरी है ना कि उसे पढ़ना-पढ़ाना क्योंकि सिर्फ़ पढ़ाने में एक पक्ष अपने विचार कहता है और दूसरा पक्ष सिर्फ़ सुनता है।
अंबेडकर विश्वविद्यालय की ही प्रोफ़ेसर रुक्मिणी सेन कहती हैं, "यह सच है कि हर महिला की स्थिति उनके वर्ग, जाति, क्षेत्र, लैंगिक झुकाव और सक्षमता-अक्षमता के आधार पर अलग है और इसलिए हम जिस फ़ेमिनिस्ट तालीम की बात कर रहें हैं, वो इन सबको ध्यान में रखते हुए अपनी समझ और अनुभव एक दूसरे से साझा करने की कोशिश है। यह ज़रूरी है कि हम महिलाओं की अलग-अलग परिस्थितियों को समझें और एक दूसरे के प्रति एकजुटता दिखाएं और बदलाव की ओर बढ़ें।"
नारीवाद या फ़ेमिनिज़्म के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये बड़े शहरों की चंद महिलाओं का मुद्दा है और उन्हीं तक सीमित है। यह सच है कि नारीवाद से जुड़े बहुत से मुद्दों के बारे में जानकारी या जागरुकता अकादमिक क्षेत्र की महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ता या बड़े शहरों की कुछ महिलाओं तक सीमित है और निश्चित तौर पर इसे और लोगों तक ले जाने की ज़रूरत है लेकिन यह कहना ग़लत होगा कि नारीवाद या फ़ेमिनिज़्म शहरों की चंद महिलाओं का मुद्दा है। क्योंकि ये हर महिला के मुद्दों का समावेश करता है और फ़ेमिनिस्ट तालीम जैसे प्रोजेक्ट इन सवालों को उठा रहें हैं।
इस प्रोजेक्ट के बारे में रुक्मिणी बताती है, "फ़ेमिनिस्ट तालीम प्रोजेक्ट कमोबेश उन्हीं विचारों पर खड़ा है जिन्हें इतने सालों से भारत में जेंडर स्टडीज़ और वूमेन स्टडीज़ विभाग में पढ़ाया जा रहा है। हम जो क्लासरूम में पढ़ाते हैं वो सिर्फ़ वहीँ तक सीमित नहीं रहता। छात्र-छात्राएं इसे लेकर अलग-अलग क्षेत्रों में जाते हैं जहां पर वो इस पर अगर बातचीत भी करते हैं तो एक तरह की जागरुकता पैदा होती है। हो सकता जब वो इन विचारों को अपने कार्यस्थलों पर या दोस्तों में साझा करें तो उन्हें कई तरह के विरोधों का सामना करना पड़े और उनके विचारों को बाक़ी लोग न समझ सकें लेकिन अगर लोग विरोध भी करते हैं तो मतलब है कि कहीं न कहीं वो इन मुद्दों पर अलग तरह से सोचना शुरू करेंगें।"
प्रो. रुक्मिणी आगे बताती हैं, "महिला आंदोलनों, महिला मुद्दों से जुड़े अलग-अलग अभियानों और महिला अधिकार समूह के ज़रिये भी लोग इन मुद्दों को समाज में अलग-अलग तबक़ों और लोगों तक ले जाते हैं महिलाओं को उनके अधिकारों और क़ानून के बारे में सचेत कराने से भी बहुत सी बातें हम समाज तक पहुंचा सकते हैं। हमें इन तरीक़ों पर और ध्यान देने की ज़रूरत है।"
प्रो. कृष्णा कहती हैं, "इस प्रोजेक्ट के ज़रिये दूर दूर से कई विचार, कई संस्थान और ख़ासतौर पर लोग एक दूसरे से जुड़ रहें हैं। लंदन और भारत के छात्र-छात्राओं ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कई समानताएं भी पाई हैं और कई तरह की विविधता भी। और इस अंतर को समझकर हर किसी के नज़रिये से नारीवाद को पढ़ना एक अनोखी पहल है।"

वो आगे कहती हैं, "विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए बच्चे अलग-अलग क्षेत्रों से आते हैं। सबकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि एक सी नहीं होती है। जब बच्चे सवाल पूछते हैं तो समझ लीजिये स्थिति आसान है। स्थिति शिक्षकों के लिए तब मुश्किल है जब वो सवाल पूछने से ख़ुद को रोकने की कोशिश करते हैं ।हमें क्लास का माहौल ऐसा बनाए रखना है जिसमें इन विषयों को पढ़ने आए बच्चे अपनी बात खुलकर रखें चाहे वो बात ग़लत ही क्यों न हो लेकिन उनका बोलना ज़रूरी है। हम अगर नारीवाद की बात कर रहें हैं तो हमें संस्थागत बदलाव लाने की ज़रूरत है जिस पर हमने बातचीत की।"
दुनियाभर में आज भी महिलाएं हिंसा और भेदभाव का शिकार हैं। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की प्रोफ़ेसर राधिका गोविंदा बताती हैं, "लैंगिक असमानता और लैंगिक हिंसा आज भी, 21वीं सदी में भी सबसे बड़ी सामाजिक चुनौतियों में से एक हैं। महिलाएं आज भी इन चुनौतियों से लड़ने का लगातार प्रयास कर रहीं हैं।"
प्रो. राधिका बताती हैं, "नारीवाद और महिलाओं से जुड़े मुद्दे को और रचनातमक तरीक़े से समझाने की कोशिश की जा रही है जिससे अकादमिक दायरे से बाहर के लोग भी इससे जुड़ें और इसे समझ सकें। एडिनबर्ग विश्विद्यालय के तीन छात्र-छात्रों को वित्तीय सहायता भी दी गई है जिससे वो वेब कॉमिक और मोबाइल आर्ट के ज़रिये भी लोगों तक पहुँच सकें।"
वो बताती हैं, "इस प्रोजेक्ट के ज़रिये महिलाओं के मुद्दों पर संवाद को बढ़ाने के लिए इसे और बेहतर समझने के लिए हम लगभग 800 लोगों से मिलें है जिनमें कई एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ता और भारत व ब्रिटेन के 19 उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्र-छात्राएं शामिल हैं। हमने इन विषयों पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तीन कार्यशालाएं, 6 जन-संवाद कार्यक्रम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किये हैं। इन कार्यक्रमों में सिर्फ़ समस्या पर ही नहीं बात की है बल्कि समाधान की तरफ़ भी क़दम उठाए गए हैं।"
हाल ही में इन विषयों पर तीन दिन की कार्यशाला अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित की गई। इसमें एडिनबर्ग विश्विद्यालय के भी शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला में महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न, हिंसा, उनके अनुभव पर बातचीत हुई। साथ ही इस पर भी बात की गई कि क्लासरूम की शिक्षा को बाहर की दुनिया से कैसे जोड़ा जा सकता है और अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
30 अक्टूबर को इस कार्यशाला में मीडिया और पब्लिशिंग हाउस में काम करने वाली महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किये। इस विषय पर बात रखने के लिए इंडियन कल्चरल फ़ोरम की हेड गीता हरिहरन, ज़ुबान पब्लिशिंग हाउस की निदेशक उर्वशी भुटालिया, अंबेडकर विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ़ लेटर्स की डीन राधा चक्रवर्ती व वरिष्ठ पत्रकार और लेखक भाषा सिंह और पामेला फ़िलोप्स भी शामिल हुईं।
इन महिलाओं ने बताया कि किस तरह से भारत का मीडिया महिलाओं के मुद्दों को हाशिये पर रखता है। महिलाओं के मुद्दों पर मीडिया में तभी बात होती है जब किसी महिला के साथ कोई हिंसा या उत्पीड़न की घटनाएं होती है। कई मीडिया संस्थानों में वूमेन डेस्क होने के बावजूद महिलाओं के ऊपर होने वाली स्टोरीज़ में संवेदनशीलता नहीं दिखाई देती।

जानी-मानी पत्रकार भाषा सिंह ने इसपर कहा, "हिंदी मीडिया की स्थिति और भी ख़राब है। महिलाओं के असली मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता, इन मुद्दों को अनदेखा किया जाता है और हाशिये पर रखा जाता है। मज़दूर वर्ग की महिलाओं और मध्य वर्ग की महिलाओं में अंतर बढ़ता जा रहा है क्योंकि इस पोस्ट ट्रुथ के समय में मीडिया जनता के लिए ज़रूरी मुद्दों को नहीं उठाता।"
उन्होंने बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत स्कीम और सरकार द्वारा घोषित नारी सशक्तिकरण से जुड़ी अन्य स्कीमों को ठीक से समझने व उनपर चर्चा करने और सवाल उठाने की ज़रूरत पर भी लोगों का ध्यान खींचा।
द वायर की पब्लिक एडिटर पामेला फ़िलोप्स ने कहा, "मीडिया एक तरह का मार्केट हो गया है जिसमें नागरिक एक कस्टमर की तरह है। मीडिया में बहुत से तबक़ों की आवाज़ें ग़ायब होती जा रही हैं।"
उन्होंने कहा अगर जनता के असल मुद्दों को मीडिया ऐसे ही दरकिनारे करता रहा तो हम और राजनितिक और आर्थिक तौर पर और मुश्किल दौर में जाएंगें।
महिलाओं के लेखन को, उनके विचारों को और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को आज भी मीडिया में उतनी जगह नहीं मिलती। अक्सर उनके साथ होने वाली हिंसाओं पर बात करके महिला मुद्दों को सीमित कर दिया जाता है। राजनीति से जुड़े मुद्दों पर अक्सर महिलाओं की राय नहीं ली जाती है। किसी भी गंभीर विषयों से जुड़ी ख़बरों को इसलिए जगह नहीं मिलती क्योंकि उस पर ज़्यादा लाइक्स नहीं आते, वो स्टोरीज़ ज़्यादा शेयर नहीं होती। वहीं महिला-विरोधी या संवेदनहीन टिप्पणी करते हुए लिखी गयी हेडलाइन तुरंत ट्रेंडिंग में अपनी जगह बना लेती है।
प्रो. रुक्मिणी कहती हैं, "हमने इस बात पर चर्चा की कि बड़े-बड़े मीडिया संस्थानों और उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं की स्थिति क्या है। निर्णय लेने में कितनी भूमिका है। आज भी लगभग हर कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है, अक्सर उन्हें सेक्सिस्ट टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन महिलाएं इन मुद्दों पर अलग अलग तरीक़ों से आवाज़ उठा रही हैं।"
प्रो.कृष्णा कहती हैं, "इस कार्यशाला के ज़रिये हम महिलाओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवाद करने की कोशिश कर रहें हैं। हम मानते हैं कि क्लासरूम में होने वाली पढ़ाई को महिला आंदोलन से जोड़ने से दोनों को ही फ़ायदा मिलता है। हम मानते हैं नवउदारवाद ने महिला आंदोलन और नारीवाद से जुड़ी शिक्षा को प्रभावित किया है।"
इस प्रोजेक्ट में अंबेडकर विश्वविद्यालय के तीन विभाग- स्कूल ऑफ़ लेटर्स, स्कूल ऑफ़ ह्यूमन स्टडीज़ और डेवेलपमेंट स्टडीज़ के छात्र-छात्राएं और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र, जेंडर स्टडीज़, अंग्रेजी साहित्य व अंतरराष्ट्रीय राजनीति विभाग के छात्र-छात्रायें शामिल हैं।
ये फ़ेमिनिस्ट तालीम की वेबसाइट है : https://feministtaleem.net/